Blog by Khushi prerna | Digital Diary
" To Present local Business identity in front of global market"
" To Present local Business identity in front of global market"
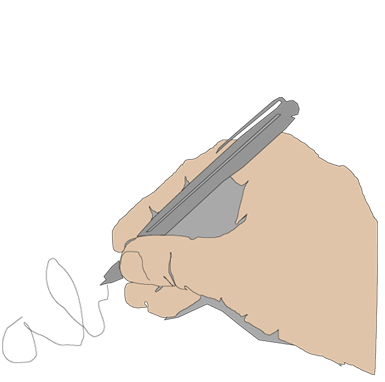 Digital Diary Submit Post
Digital Diary Submit Post
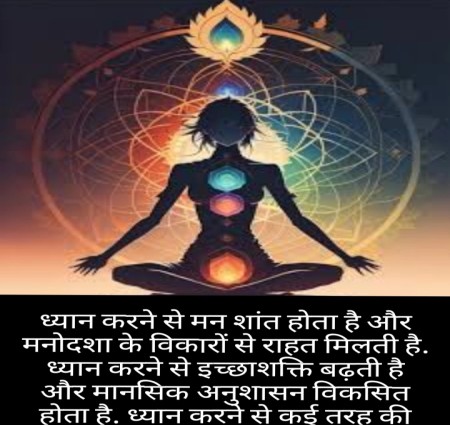 हाल के वर्षों में, ध्यान की लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके लाभों के बारे में जानते हैं। वास्तव में, यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने और आपके विचारों को केंद्रित करने और पुनर्निर्देशित करने में मदद करता है। यह आपको अपने आस-पास और खुद के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। बहुत से लोग अपने तनाव के स्तर को कम करने और गहरी एकाग्रता विकसित करने के लिए ध्यान का उपयोग करते हैं।...
Read More
हाल के वर्षों में, ध्यान की लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके लाभों के बारे में जानते हैं। वास्तव में, यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने और आपके विचारों को केंद्रित करने और पुनर्निर्देशित करने में मदद करता है। यह आपको अपने आस-पास और खुद के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। बहुत से लोग अपने तनाव के स्तर को कम करने और गहरी एकाग्रता विकसित करने के लिए ध्यान का उपयोग करते हैं।...
Read More
हाल के वर्षों में, ध्यान की लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके लाभों के बारे में जानते हैं। वास्तव में, यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने और आपके विचारों को केंद्रित करने और पुनर्निर्देशित करने में मदद करता है।
यह आपको अपने आस-पास और खुद के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। बहुत से लोग अपने तनाव के स्तर को कम करने और गहरी एकाग्रता विकसित करने के लिए ध्यान का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, बहुत से लोग ध्यान का उपयोग अन्य लाभकारी भावनाओं और आदतों को विकसित करने के लिए भी करते हैं, जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वस्थ नींद पैटर्न, आत्म-अनुशासन और यहां तक कि बेहतर दर्द सहनशीलता।
यहां ध्यान के 12 विज्ञान-आधारित लाभ बताए गए हैं।
ध्यान करने से मन शांत होता है और मनोदशा के विकारों से राहत मिलती है. ध्यान करने से इच्छाशक्ति बढ़ती है और मानसिक अनुशासन विकसित होता है. ध्यान करने से कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है
Read Full Blog...आर्तध्यान
आर्त का अर्थ है- पीड़ा या दु:ख। प्रिय व्यक्ति या वस्तु के वियोग और अप्रिय व्यक्ति या वस्तु के संयोग से होनेवाली मानसिक विकलता की स्थिति में जो चिन्तन होता है, वह आर्तध्यान कहलाता है। वेदनाजनित आकुलता और विषयसुख की प्राप्ति के लिए किया जानेवाला दृढ़ संकल्प भी इसी ध्यान का अंग है। व्याकुलता, छटपटाहट और अधीरता आर्त्तध्यान की निष्पत्तियाँ हैं। आर्त्तध्यान के चार भेद हैं-
1 इष्टवियोग- प्रिय व्यक्ति या वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए होनेवाली वियोगजन्य विकलता।
2 अनिष्टसंयोग- अप्रिय व्यक्ति या वस्तु के संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए होनेवाली संयोगजन्य विकलता।
3 पीड़ाचिन्तन- वेदनाजन्य आतुरता, छटपटाहट
4 निदान- भावी भोगों की आकांक्षाजन्य आतुरता।
Read Full Blog...
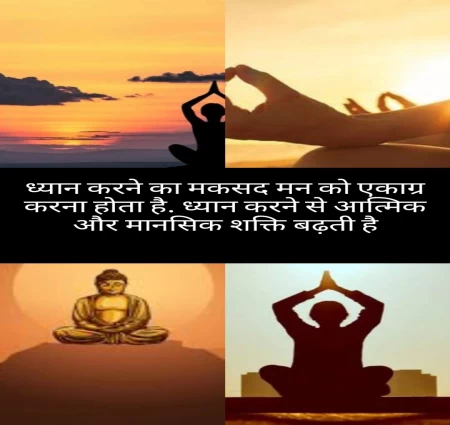 ध्यान कई तरह के होते हैं. ध्यान करने के कुछ तरीके और प्रकार ध्यान कई तरह के होते हैं. ध्यान करने के कुछ तरीके ये रहे: आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्लध्यान, माइंडफ़ुलनेस मेडिटेशन, करुणा ध्यान, एकाग्रता ध्यान, जेन ध्यान, विपश्यना ध्यान, प्रेम-दया ध्यान. ध्यान करने के कुछ और तरीके: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, निर्देशित ध्यान. ध्यान करने से शारीरिक, आध्यात्मिक, और भा...
Read More
ध्यान कई तरह के होते हैं. ध्यान करने के कुछ तरीके और प्रकार ध्यान कई तरह के होते हैं. ध्यान करने के कुछ तरीके ये रहे: आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्लध्यान, माइंडफ़ुलनेस मेडिटेशन, करुणा ध्यान, एकाग्रता ध्यान, जेन ध्यान, विपश्यना ध्यान, प्रेम-दया ध्यान. ध्यान करने के कुछ और तरीके: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, निर्देशित ध्यान. ध्यान करने से शारीरिक, आध्यात्मिक, और भा...
Read More
ध्यान कई तरह के होते हैं. ध्यान करने के कुछ तरीके और प्रकार
ध्यान कई तरह के होते हैं. ध्यान करने के कुछ तरीके ये रहे:
आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्लध्यान, माइंडफ़ुलनेस मेडिटेशन, करुणा ध्यान, एकाग्रता ध्यान, जेन ध्यान, विपश्यना ध्यान, प्रेम-दया ध्यान.
ध्यान करने के कुछ और तरीके: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, निर्देशित ध्यान.
ध्यान करने से शारीरिक, आध्यात्मिक, और भावनात्मक सेहत में सुधार होता है. यह घबराहट और अवसाद को कम करता है. ध्यान करने से तनाव, रक्तचाप, और डर की भावना कम होती है.
ध्यान करने के लिए आप ऐप, वेबसाइट, या स्थानीय कक्षाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
ध्यान के कई प्रकार होते हैं. ध्यान के कुछ प्रमुख प्रकार ये रहे:
विपश्यना ध्यान: यह बौद्ध और भारतीय परंपरा का एक ध्यान है. इसमें विचारों को रोकने की कला सीखी जाती है.
प्रेम-कृपा ध्यान: इसमें प्यार और दया की भावना को जगाया जाता है.
कंसेंट्रेटिव ध्यान: इसमें किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.
माइंडफ़ुलनेस ध्यान: यह संज्ञानात्मक चिकित्सा का एक रूप है. इसमें मौजूदा स्थिति में जागरूक रहना होता है.
शांतिदायक ध्यान: यह ध्यान तनावपूर्ण विचारों को कम करने और मानसिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है.
अंतर्दृष्टि ध्यान: इसे विपश्यना भी कहा जाता है. इसमें विचारों और भावनाओं की आंतरिक समझ हासिल की जाती है.
वन ध्यान: इसमें प्रकृति में रहकर जंगल के दृश्य और ध्वनियों का आनंद लिया जाता है.
त्राटक ध्यान: इसमें किसी एक बिंदु पर एकटक देखा जाता है.
प्राणायाम ध्यान: यह योग का एक हिस्सा है. इसमें सांस नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.
ज़ेन ध्यान: यह बैठकर किया जाने वाला ध्यान है. इसमें जागरूकता के साथ विचारों का अवलोकन किया जाता है.
स्वास्थ्य और खुशहाली बढ़ाने के लिए ध्यान
Read Full Blog... अपने शारीरिक शरीर का ख्याल रखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मन और शरीर जटिल तरीकों से एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शारीरिक बीमारी आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रबंधित करना अधिक कठिन बना सकती है। तनाव, ऊर्जा की कमी, खराब नींद और अन्य समस्याएं भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। इस लेख में बताया गया है कि आपको अपने शरीर का ख्याल क्यों रखना चाहिए और...
Read More
अपने शारीरिक शरीर का ख्याल रखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मन और शरीर जटिल तरीकों से एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शारीरिक बीमारी आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रबंधित करना अधिक कठिन बना सकती है। तनाव, ऊर्जा की कमी, खराब नींद और अन्य समस्याएं भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। इस लेख में बताया गया है कि आपको अपने शरीर का ख्याल क्यों रखना चाहिए और...
Read More
अपने शारीरिक शरीर का ख्याल रखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मन और शरीर जटिल तरीकों से एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शारीरिक बीमारी आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रबंधित करना अधिक कठिन बना सकती है। तनाव, ऊर्जा की कमी, खराब नींद और अन्य समस्याएं भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं।
इस लेख में बताया गया है कि आपको अपने शरीर का ख्याल क्यों रखना चाहिए और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि आप खुद की बेहतर देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं।
ऐसे कई कारण हैं कि आपके शरीर की देखभाल करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है:
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कामकाज को प्रभावित करती हैं : स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चाहे वे छोटी ही क्यों न हों, आपके जीवन के अन्य पहलुओं में हस्तक्षेप कर सकती हैं या उन्हें प्रभावित भी कर सकती हैं। दर्द, पीड़ा, सुस्ती और अपच जैसी अपेक्षाकृत छोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी आपकी खुशी और तनाव के स्तर पर असर डालती हैं।
खराब स्वास्थ्य आदतें आपके जीवन में तनाव बढ़ा सकती हैं : वे इस बात में भी भूमिका निभाती हैं कि आप तनाव से कितनी अच्छी तरह निपट पाते हैं। खराब स्वास्थ्य से होने वाला तनाव बहुत ज़्यादा होता है।
खराब स्वास्थ्य दैनिक जीवन में बाधा डालता है : स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ दैनिक कार्यों को अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं, वित्तीय तनाव पैदा कर सकती हैं और यहाँ तक कि आपकी जीविका कमाने की क्षमता को भी खतरे में डाल सकती हैं।
तनाव से स्वास्थ्य खराब हो सकता है : तनाव से सामान्य सर्दी से लेकर अधिक गंभीर स्थितियों और बीमारियों तक की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए स्वस्थ आदतें बनाए रखना लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। यह लेख कुछ स्वस्थ आदतों पर नज़र डालता है जिनका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
आपको ऐसे खाद्य पदार्थ खाने की प्रतिबद्धता भी दिखानी चाहिए जो आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाएँ और आपके सिस्टम को सुचारू रूप से चलाते रहें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो खाते हैं वह न केवल आपके अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह आपके तनाव के स्तर को भी प्रभावित कर सकता है ।
अगर आप भूखे या कुपोषित हैं तो तनाव से निपटना बहुत मुश्किल है। भूख आपको तनाव के प्रति भावनात्मक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील बना सकती है, जिससे आप छोटी-छोटी दैनिक परेशानियों के सामने चिड़चिड़े या यहां तक कि क्रोधित हो सकते हैं। आप क्या खाते हैं, इस पर नज़र रखना तनाव प्रबंधन उपकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य रक्षक भी हो सकता है।
स्वास्थ्य और खुशहाली बढ़ाने के लिए ध्यान
Read Full Blog...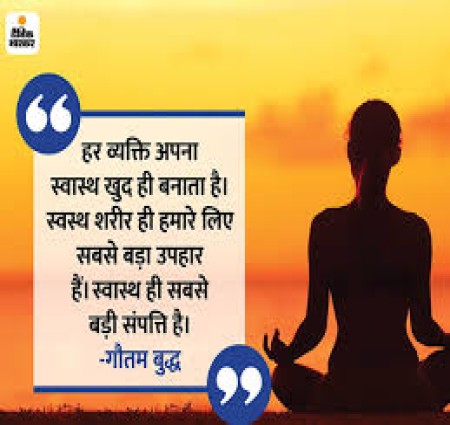 अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का हृदय और मशाल लोगोअमेरिकन हार्ट एसोसिएशन मेनू दिल का दौरा और स्ट्रोक के लक्षण सीपीआर सीखें स्वयंसेवक शॉपहार्ट घर स्वस्थ रहन - सहन स्वस्थ जीवन शैली मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण स्वास्थ्य और खुशहाली बढ़ाने के लिए ध्यान स्वास्थ्य और खुशहाली बढ़ाने के लिए ध्यान ध्यान माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करने से आपको तनाव और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने, बेहतर नींद लेने,...
Read More
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का हृदय और मशाल लोगोअमेरिकन हार्ट एसोसिएशन मेनू दिल का दौरा और स्ट्रोक के लक्षण सीपीआर सीखें स्वयंसेवक शॉपहार्ट घर स्वस्थ रहन - सहन स्वस्थ जीवन शैली मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण स्वास्थ्य और खुशहाली बढ़ाने के लिए ध्यान स्वास्थ्य और खुशहाली बढ़ाने के लिए ध्यान ध्यान माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करने से आपको तनाव और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने, बेहतर नींद लेने,...
Read More
माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करने से आपको तनाव और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने, बेहतर नींद लेने, अधिक संतुलित और जुड़ा हुआ महसूस करने और यहां तक कि हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास हैं - अक्सर सांस लेने, शांत चिंतन या किसी चीज़ पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने का उपयोग करते हुए, जैसे कि कोई छवि, वाक्यांश या ध्वनि - जो आपको तनाव से मुक्त होने और अधिक शांत और शांतिपूर्ण महसूस करने में मदद करते हैं। इसे अपने जीवन में तनाव से एक छोटी छुट्टी के रूप में सोचें! तनाव आपके शरीर का प्राकृतिक अलार्म सिस्टम है। यह एड्रेनालाईन नामक एक हार्मोन जारी करता है जो आपकी सांसों की गति बढ़ाता है और आपकी हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाता है। यह हमें कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है, जो एक अच्छी बात हो सकती है जब हम किसी वास्तविक खतरे या प्रदर्शन की आवश्यकता का सामना कर रहे हों।
लेकिन यह "लड़ो या भागो" प्रतिक्रिया आपके शरीर पर भारी पड़ सकती है जब यह बहुत लंबे समय तक चलती है या एक नियमित घटना है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन तनाव को स्वस्थ तरीके से संभालने का एक तरीका प्रदान करता है।
_1738304509.jpeg) ध्यान से स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है
ध्यान से स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता हैहाल ही में किए गए अध्ययनों में रक्तचाप को कम करने में ध्यान के प्रभाव के बारे में आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि यह लोगों को अनिद्रा, अवसाद और चिंता से निपटने में मदद कर सकता है।
कुछ शोध बताते हैं कि ध्यान मस्तिष्क में शारीरिक परिवर्तन लाता है और इससे निम्नलिखित में मदद मिल सकती है:
सूचना को संसाधित करने की क्षमता बढ़ाएँ.
उम्र बढ़ने के संज्ञानात्मक प्रभावों को धीमा करें।
सूजन कम करें.
प्रतिरक्षा प्रणाली को सहायता प्रदान करें।
रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम करें।
दर्द के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें।
नींद में सुधार करें.
स्वास्थ्य और खुशहाली बढ़ाने के लिए ध्यान
Read Full Blog... मेडिटेशन में क्या सोचना चाहिए? मेडिटेशन या ध्यान करते समय केवल सर्व शक्तिमान ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो इस पूरी सृष्टि का स्वामी है , जो निराकार है , उसका कोई रूप या आकृति नहीं है जो हर समय हमारे साथ है। वही सारी शक्तियों का स्रोत है ध्यान के दौरान कहां फोकस करना है? भौंहों के बीच का बिंदु, या आध्यात्मिक आँख , शरीर में एकाग्रता का स्थान है, और जब भी हमें गहराई से ध्यान के...
Read More
मेडिटेशन में क्या सोचना चाहिए? मेडिटेशन या ध्यान करते समय केवल सर्व शक्तिमान ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो इस पूरी सृष्टि का स्वामी है , जो निराकार है , उसका कोई रूप या आकृति नहीं है जो हर समय हमारे साथ है। वही सारी शक्तियों का स्रोत है ध्यान के दौरान कहां फोकस करना है? भौंहों के बीच का बिंदु, या आध्यात्मिक आँख , शरीर में एकाग्रता का स्थान है, और जब भी हमें गहराई से ध्यान के...
Read More
मेडिटेशन में क्या सोचना चाहिए?
मेडिटेशन या ध्यान करते समय केवल सर्व शक्तिमान ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो इस पूरी सृष्टि का स्वामी है , जो निराकार है , उसका कोई रूप या आकृति नहीं है जो हर समय हमारे साथ है। वही सारी शक्तियों का स्रोत है
ध्यान के दौरान कहां फोकस करना है?
भौंहों के बीच का बिंदु, या आध्यात्मिक आँख , शरीर में एकाग्रता का स्थान है, और जब भी हमें गहराई से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, तो हम स्वाभाविक रूप से वहाँ ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान के दौरान, बिना किसी तनाव के, आँखों को ऊपर उठाकर रखना बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप अपनी एकाग्रता में सुधार देखेंगे।
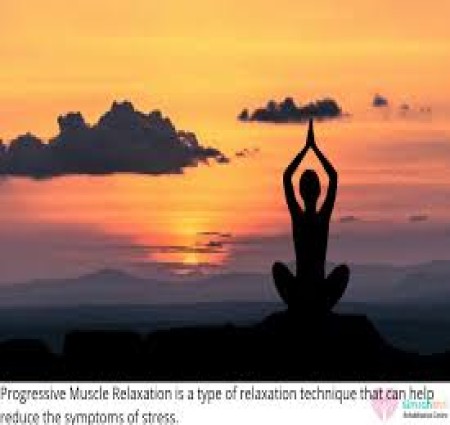 कभी-कभी तनाव महसूस करना सामान्य बात है। लेकिन अगर आपका तनाव बढ़ता है, या यह लंबे समय तक जारी रहता है, तो आपकी मांसपेशियों में तनाव हो सकता है। आपको बिना एहसास के भी मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है। मांसपेशियों में तनाव दूर करने का एक तरीका प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम करना है, जिसे जैकबसन की विश्राम तकनीक के रूप में भी जाना जाता है । प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम (पीएमआर) एक प्रकार की थेरेपी है जिसमें...
Read More
कभी-कभी तनाव महसूस करना सामान्य बात है। लेकिन अगर आपका तनाव बढ़ता है, या यह लंबे समय तक जारी रहता है, तो आपकी मांसपेशियों में तनाव हो सकता है। आपको बिना एहसास के भी मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है। मांसपेशियों में तनाव दूर करने का एक तरीका प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम करना है, जिसे जैकबसन की विश्राम तकनीक के रूप में भी जाना जाता है । प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम (पीएमआर) एक प्रकार की थेरेपी है जिसमें...
Read More
कभी-कभी तनाव महसूस करना सामान्य बात है। लेकिन अगर आपका तनाव बढ़ता है, या यह लंबे समय तक जारी रहता है, तो आपकी मांसपेशियों में तनाव हो सकता है। आपको बिना एहसास के भी मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है।
मांसपेशियों में तनाव दूर करने का एक तरीका प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम करना है, जिसे जैकबसन की विश्राम तकनीक के रूप में भी जाना जाता है । प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम (पीएमआर) एक प्रकार की थेरेपी है जिसमें एक समय में एक विशिष्ट पैटर्न में आपके मांसपेशी समूहों को कसना और आराम करना शामिल है।
इसका लक्ष्य आपकी मांसपेशियों से तनाव को मुक्त करना है, साथ ही आपको यह पहचानने में मदद करना है कि तनाव कैसा महसूस होता है।
नियमित रूप से अभ्यास करने पर, यह तकनीक आपको तनाव के शारीरिक प्रभावों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। शोध में यह भी पाया गया है कि इसके निम्नलिखित स्थितियों के लिए चिकित्सीय लाभ हैं:
सदस्यता लें
पोषण
भोजन किट
विशेष आहार
पौष्टिक भोजन
भोजन स्वतंत्रता
स्थितियाँ
अच्छा महसूस कराता भोजन
उत्पादों
विटामिन और पूरक
वहनीयता
वज़न प्रबंधन
प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम के लाभ और इसे कैसे करें
चिकित्सकीय रूप से ग्रेगरी मिनिस, डीपीटी , फिजिकल थेरेपी द्वारा समीक्षा की गई -10 अगस्त, 2020 को कर्स्टन नुनेज़ द्वारा लिखित
पीएमआर के बारे में
फ़ायदे
इसे कैसे करना है
शुरुआती सुझाव
जमीनी स्तर
कभी-कभी तनाव महसूस करना सामान्य बात है। लेकिन अगर आपका तनाव बढ़ता है, या यह लंबे समय तक जारी रहता है, तो आपकी मांसपेशियों में तनाव हो सकता है। आपको बिना एहसास के भी मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है।
मांसपेशियों में तनाव दूर करने का एक तरीका प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम करना है, जिसे जैकबसन की विश्राम तकनीक के रूप में भी जाना जाता है । प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम (पीएमआर) एक प्रकार की थेरेपी है जिसमें एक समय में एक विशिष्ट पैटर्न में आपके मांसपेशी समूहों को कसना और आराम करना शामिल है।
इसका लक्ष्य आपकी मांसपेशियों से तनाव को मुक्त करना है, साथ ही आपको यह पहचानने में मदद करना है कि तनाव कैसा महसूस होता है।
नियमित रूप से अभ्यास करने पर, यह तकनीक आपको तनाव के शारीरिक प्रभावों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। शोध में यह भी पाया गया है कि इसके निम्नलिखित स्थितियों के लिए चिकित्सीय लाभ हैं:
उच्च रक्तचाप
आधासीसी
नींद संबंधी समस्याएं
आइये जानें कि पीएमआर क्या है, इसके क्या लाभ हैं, तथा इस तकनीक का प्रयोग कैसे किया जाता है।
प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम क्या है?
पीएमआर की रचना अमेरिकी चिकित्सक एडमंड जैकबसन ने 1920 के दशक में की थी। यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि शारीरिक विश्राम मानसिक विश्राम को बढ़ावा दे सकता है।
जैकबसन ने पाया कि आप मांसपेशियों को तनाव देकर और फिर उन्हें ढीला करके आराम दे सकते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि ऐसा करने से दिमाग को आराम मिलता है।
पीएमआर विश्राम की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके लिए आपको एक समय में एक मांसपेशी समूह पर काम करना होता है। इससे आप उस विशिष्ट क्षेत्र में तनाव को नोटिस कर सकते हैं।
आराम करने से पहले प्रत्येक मांसपेशी समूह को तनाव देना भी आवश्यक है । यह क्रिया क्षेत्र में विश्राम की भावना पर जोर देती है।
Read Full Blog...
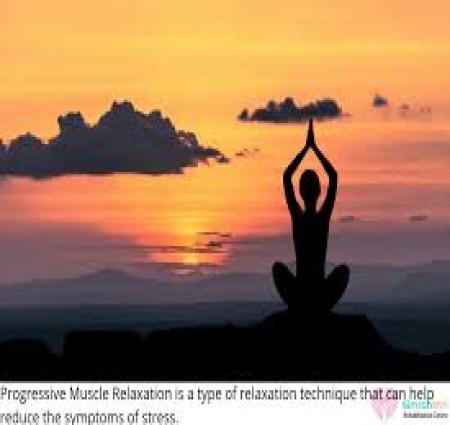 मेडिटेशन का अभ्यास करना एक ऐसी साधना है जो हमारे जीवन को सही दिशा देने और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। खासकर, सुबह ध्यान लगाने के बहुत सारे फायदे हैं जो हमें न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी फायदा पहुंचाता है। इस लेख में, हम जानेंगे कि सुबह ध्यान लगाने से क्या फायदे मिलते हैं। मानसिक शांति और स्थिरता अगर भविष्य में सफल होना है तो सबसे पहले मानसिक शांति और मन की स्थिरता जरूरी है। मन...
Read More
मेडिटेशन का अभ्यास करना एक ऐसी साधना है जो हमारे जीवन को सही दिशा देने और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। खासकर, सुबह ध्यान लगाने के बहुत सारे फायदे हैं जो हमें न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी फायदा पहुंचाता है। इस लेख में, हम जानेंगे कि सुबह ध्यान लगाने से क्या फायदे मिलते हैं। मानसिक शांति और स्थिरता अगर भविष्य में सफल होना है तो सबसे पहले मानसिक शांति और मन की स्थिरता जरूरी है। मन...
Read More
मेडिटेशन का अभ्यास करना एक ऐसी साधना है जो हमारे जीवन को सही दिशा देने और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। खासकर, सुबह ध्यान लगाने के बहुत सारे फायदे हैं जो हमें न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी फायदा पहुंचाता है। इस लेख में, हम जानेंगे कि सुबह ध्यान लगाने से क्या फायदे मिलते हैं।
अगर भविष्य में सफल होना है तो सबसे पहले मानसिक शांति और मन की स्थिरता जरूरी है। मन बड़ा चंचल होता है जिसने इसे नियंत्रित कर लिया वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है और कहीं भी पहुंच सकता है लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मन की गति इतनी तेज़ होती है कि इस पर कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यही कारण है कि ऋषि मुनियों और बड़े-बड़े ज्ञानियों ने ध्यान को मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा टूल बताया है। ध्यान लगाने से मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन बड़े से बड़े फैसले करने में सहज और सक्षम होता है।
सुबह-सुबह आप जो करेंगे उसका असर आपके पूरे दिन पर रहता है इसलिए अगर आप खुद से कनेक्ट होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप खुद को जान सकें तो सुबह ध्यान जरूर लगाएं। ये पूरा दिन आपका आपसे कनेक्शन बनाए रखता है। ध्यान के जरिए आप जीवन के मूल्यों को समझते हैं। इससे आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो कितने ही सफल हो जाओ कोई फायदा नहीं। सुबह-सुबह जो लोग प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन ना करने वालों के मुकाबले बीमारियों से दूर रहते हैं। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। मेडिटेशन के दौरान हम गहरी सांस लेते हैं तो परिणामस्वरूप, हमारा दिल और श्वसन प्रणाली मजबूत रहती है।
Read Full Blog...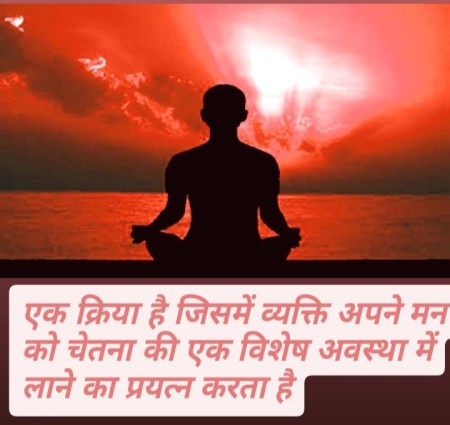 ध्यान से क्या अभिप्राय है ध्यान क्या है? ध्यान एक अभ्यास है जिसमें मानसिक और शारीरिक तकनीकों के संयोजन का उपयोग करके अपने दिमाग को केंद्रित या साफ़ करना शामिल है । आपके द्वारा चुने गए ध्यान के प्रकार के आधार पर, आप आराम करने, चिंता और तनाव को कम करने और बहुत कुछ करने के लिए ध्यान कर सकते हैं। ध्यान यदि ने किसी भी चीज या कार्य पर एकाग्र होना । जितने तुम एकाग्र होगे उतने तुम उसमे डूबते जाओगे और वह ख...
Read More
ध्यान से क्या अभिप्राय है ध्यान क्या है? ध्यान एक अभ्यास है जिसमें मानसिक और शारीरिक तकनीकों के संयोजन का उपयोग करके अपने दिमाग को केंद्रित या साफ़ करना शामिल है । आपके द्वारा चुने गए ध्यान के प्रकार के आधार पर, आप आराम करने, चिंता और तनाव को कम करने और बहुत कुछ करने के लिए ध्यान कर सकते हैं। ध्यान यदि ने किसी भी चीज या कार्य पर एकाग्र होना । जितने तुम एकाग्र होगे उतने तुम उसमे डूबते जाओगे और वह ख...
Read More
ध्यान क्या है? ध्यान एक अभ्यास है जिसमें मानसिक और शारीरिक तकनीकों के संयोजन का उपयोग करके अपने दिमाग को केंद्रित या साफ़ करना शामिल है । आपके द्वारा चुने गए ध्यान के प्रकार के आधार पर, आप आराम करने, चिंता और तनाव को कम करने और बहुत कुछ करने के लिए ध्यान कर सकते हैं।
ध्यान यदि ने किसी भी चीज या कार्य पर एकाग्र होना । जितने तुम एकाग्र होगे उतने तुम उसमे डूबते जाओगे और वह खिलके बाहर आएगा। ध्यान अध्यात्मिकता की वह कड़ी है जो तुमको तुम्हारे सही अस्तित्व से जोड़ती है और आखिर में ईश्वर तक जोड़ देती है । यह तक की पतंजलि के द्वारा विरचित अष्टांग योग में भी ध्यान की अहम भूमिका है
एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता ह
Inhe bhi padhe
Read Full Blog...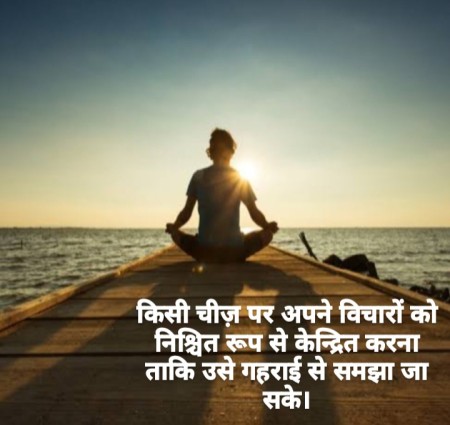 मेडिटेशन का क्या अर्थ है ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने-आप में एक लक्ष्य हो सकता है। 'ध्यान' से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। ध्यान या मेडिटेशन का मतलब है, अपने दिमाग को केंद्रित करना या साफ़ करना. यह एक अभ्यास है जिसमें मानसिक और शारीरिक तकनी...
Read More
मेडिटेशन का क्या अर्थ है ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने-आप में एक लक्ष्य हो सकता है। 'ध्यान' से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। ध्यान या मेडिटेशन का मतलब है, अपने दिमाग को केंद्रित करना या साफ़ करना. यह एक अभ्यास है जिसमें मानसिक और शारीरिक तकनी...
Read More
मेडिटेशन का क्या अर्थ है
ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने-आप में एक लक्ष्य हो सकता है। 'ध्यान' से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है।
ध्यान या मेडिटेशन का मतलब है, अपने दिमाग को केंद्रित करना या साफ़ करना. यह एक अभ्यास है जिसमें मानसिक और शारीरिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है. ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और दिमाग में ऊर्जा और सकारात्मकता आती है.
ध्यान करने का अर्थ है किसी चीज़ पर अपने विचारों को निश्चित रूप से केन्द्रित करना ताकि उसे गहराई से समझा जा सके।
ध्यान करने के फ़ायदे:
ध्यान करने से चिंता और तनाव कम होता है.
ध्यान करने से एकाग्रता, स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास, और इच्छा शक्ति बढ़ती है.
ध्यान करने से थकान कम होती है.
ध्यान करने से दिमाग को ऊर्जा मिलती है.
ध्यान करने का तरीका:
ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके या नीचे की ओर टकटकी लगाकर चुपचाप बैठना या आराम करना होता है.
ध्यान करने के लिए मानसिक और शारीरिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है.
Read Full Blog...