मानव व्यवहार और व्यक्तित्व: आलस्य, व्यक्तित्व और आदतों के मनोवैज्ञानिक पहलू हम सभी के जीवन में सोच, निर्णय और व्यवहार का गहरा प्रभाव होता है। मानव व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम क्यों वैसा करते हैं जैसा करते हैं, और हमारी आदतें और सोच हमारे जीवन को कैसे आकार देती हैं। इस ब्लॉग में हम तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देंगे: आलस्य (Procrastination), इंट्रोवर्ट और ए...
Read More
मानव व्यवहार और व्यक्तित्व: आलस्य, व्यक्तित्व और आदतों के मनोवैज्ञानिक पहलू
हम सभी के जीवन में सोच, निर्णय और व्यवहार का गहरा प्रभाव होता है। मानव व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम क्यों वैसा करते हैं जैसा करते हैं, और हमारी आदतें और सोच हमारे जीवन को कैसे आकार देती हैं। इस ब्लॉग में हम तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देंगे: आलस्य (Procrastination), इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्ट व्यक्तित्व, और आदतों का निर्माण और परिवर्तन।
1. आलस्य (Procrastination) के मनोवैज्ञानिक कारण
आलस्य या Procrastination वह प्रवृत्ति है जिसमें हम आवश्यक कार्यों को टालते रहते हैं, चाहे उन्हें करना कितना भी जरूरी क्यों न हो। यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सफलता पर भी असर डालता है।
मुख्य कारण:
1. डर और असफलता का भय:
लोग अक्सर काम शुरू करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सफल नहीं होंगे।
उदाहरण: एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी टालता है क्योंकि उसे डर है कि वह अच्छे अंक नहीं ला पाएगा।
2. परफेक्शनिज़्म
सब कुछ सही होना चाहिए" की सोच काम को शुरू करने में बाधा डालती है।
उदाहरण: लेखक जो किताब लिखना चाहता है, लेकिन हर शब्द पर सही होने की चिंता में महीनों तक लिखना टालता रहता है।
3. ऊर्जा और ध्यान की कमी:
मानसिक थकान या ध्यान की कमी भी आलस्य बढ़ाती है।
उदाहरण: लंबे काम के बाद व्यक्ति नए कार्यों को टालता है।
4. प्रोत्साहन की कमी:
जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता या प्रेरणा कमजोर होती है, तो काम टलता है।
उपाय और टिप्स:
बड़े कार्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटें।
समय सीमा (Deadline) तय करें।
खुद को छोटे इनाम और प्रोत्साहन दें।
ध्यान और ऊर्जा बनाए रखने के लिए ब्रेक और आराम लें।
2. इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्ट व्यक्तित्व
हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। यह निर्धारित करता है कि हम सोचते कैसे हैं, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और जीवन में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं।
इंट्रोवर्ट
अकेले समय बिताने से ऊर्जा मिलती है।
गहरी सोच और आत्म-विश्लेषण में बेहतर।
शांत, गंभीर और एकाग्र।
उदाहरण: कोई व्यक्ति जो मीटिंग्स में कम बोलता है, लेकिन अकेले काम करने में उत्कृष्ट होता है।
एक्स्ट्रोवर्ट
सामाजिक इंटरैक्शन से ऊर्जा मिलती है।
सक्रिय, मिलनसार और टीम में अच्छे।
जल्दी निर्णय लेने और नए अवसर अपनाने में सहज।
उदाहरण: टीम प्रोजेक्ट में दूसरों को प्रेरित करना और नेतृत्व करना।
ध्यान देने योग्य बातें
कोई भी व्यक्तित्व बेहतर या खराब नहीं होता।
दोनों के अपने फायदे और चुनौतियाँ होती हैं।
सफलता का राज अपने व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करना और अपनी शक्तियों का उपयोग करना है।
3. आदतें क्यों बनती हैं और कैसे बदलती हैं
आदतें हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार का आधार होती हैं। ये मस्तिष्क में दोहराव और ट्रिगर के कारण ऑटोमैटिक बन जाती हैं।
आदते कैसे बनती है
किसी कार्य को लगातार दोहराना।
किसी परिस्थिति या ट्रिगर के साथ व्यवहार को जोड़ना।
मस्तिष्क इसे ऑटोमैटिक पैटर्न में बदल देता है।
अच्छी आदतो के उदाहरण
रोज़ सुबह व्यायाम करना।
ध्यान या मेडिटेशन करना।
समय पर सोना और जागना।
बुरी आदत के उदाहरण
देर तक फोन इस्तेमाल करना।
अनियमित खान-पान।
आलस्य और टालमटोल।
आदत बदलने के मनोवैज्ञानिक तरीके:
1. छोटे कदमों से शुरुआत करें: बड़े बदलाव से डरने की बजाय छोटे बदलाव अपनाएं।
2. ट्रिगर और रूटीन पहचानें: समझें कौन सी परिस्थितियां आपकी आदत को ट्रिगर करती
3. इनाम और प्रोत्साहन: नई आदत पूरी करने पर खुद को इनाम दें।
4. निरंतर अभ्यास और धैर्य: आदत बदलने में समय लगता है, रोज़ अभ्यास करें।
उदाहरण
अगर आप हर रात सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो इसे धीरे-धीरे 10 मिनट पहले छोड़ना शुरू करें।
नई आदत को अपनी दिनचर्या में जोड़ें और सफलता का जश्न मनाएं।
Read Full Blog...
? मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) से जुड़े विषय 1. तनाव (Stress) क्या है और इसे कैसे कम करें? तनाव हमारे शरीर और मन की वह प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब हम किसी दबाव, चुनौती या बदलाव का सामना करते हैं। थोड़ा बहुत तनाव सामान्य है - यह हमें सक्रिय रखता है, लेकिन जब तनाव ज़्यादा बढ़ जाए, तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से नुकसान पहुँचाता है। तनाव के लक्षण: नींद न आना या ज़्यादा सोना चिड़चिड़ापन औ...
Read More
? मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) से जुड़े विषय
1. तनाव (Stress) क्या है और इसे कैसे कम करें?
तनाव हमारे शरीर और मन की वह प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब हम किसी दबाव, चुनौती या बदलाव का सामना करते हैं। थोड़ा बहुत तनाव सामान्य है - यह हमें सक्रिय रखता है, लेकिन जब तनाव ज़्यादा बढ़ जाए, तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से नुकसान पहुँचाता है।
तनाव के लक्षण:
नींद न आना या ज़्यादा सोना
चिड़चिड़ापन और गुस्सा
सिरदर्द या थकान
ध्यान केंद्रित न कर पाना
तनाव कम करने के उपाय:
रोज़ाना कम से कम 15–20 मिनट ध्यान करें
गहरी साँस लें और योग करें
अपनी दिनचर्या में मनपसंद चीज़ें शामिल करें (संगीत, किताबें, टहलना)
दोस्तों और परिवार से बात करें
मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लें
2. डिप्रेशन के लक्षण और उससे उबरने के तरीके
डिप्रेशन सिर्फ़ "उदासी" नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक निराशा, खालीपन और नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है।
मुख्य लक्षण:
लगातार उदासी या रुचि की कमी
भूख या नींद में बदलाव
खुद को बेकार महसूस करना
आत्मघाती विचार
उबरने के तरीके:
किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से मदद लें
छोटी-छोटी चीज़ों में ख़ुशी ढूँढें
अपने विचारों को लिखें (Journal लिखना बहुत मददगार है)
शरीर को सक्रिय रखें - सुबह टहलना, एक्सरसाइज़
परिवार या दोस्तों से दूरी न बनाएं
3. एंग्जायटी के संकेत और घरेलू उपाय
एंग्जायटी का मतलब है - भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता या डर। कभी-कभी ये चिंता इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति सामान्य काम भी नहीं कर पाता।
संकेत
दिल की धड़कन तेज़ होना
पसीना आना
घबराहट या डर का अहसास
सोने में कठिनाई
घरेलू उपाय
धीरे-धीरे गहरी साँस लें
कैफीन (चाय, कॉफी) कम करें
नियमित योग और मेडिटेशन करें
नींद पूरी लें
"माइंडफुलनेस" यानी वर्तमान क्षण में रहना सीखें
4. सेल्फ-केयर क्यों ज़रूरी है?
सेल्फ-केयर का मतलब है - खुद का ख्याल रखना, अपनी मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतों को समझना।
हम अक्सर दूसरों की देखभाल में खुद को भूल जाते हैं, जबकि आत्म-देखभाल हमें ऊर्जावान और खुश रखती है।
सेल्फ-केयर के तरीके
दिन में थोड़ा "मी-टाइम" निकालें
अपनी सीमाएँ तय करें - "ना" कहना सीखें
पौष्टिक भोजन और पर्याप्त नींद लें
अपने शौक पूरे करें (ड्रॉइंग, पढ़ना, संगीत आदि)
अपने मन की बात किसी विश्वसनीय व्यक्ति से शेयर करें
5. नींद और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध
नींद और मानसिक स्वास्थ्य का गहरा रिश्ता है। अगर नींद पूरी नहीं होती, तो दिमाग थक जाता है, मूड खराब रहता है और चिंता या अवसाद जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं।
कम नींद के दुष्प्रभाव
ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल
चिड़चिड़ापन
याददाश्त कम होना
डिप्रेशन या एंग्जायटी का खतरा बढ़ना
अच्छी नींद के प्रभाव
रोज़ एक ही समय पर सोएँ और उठें
सोने से पहले मोबाइल, टीवी आदि से दूरी रखें
कमरे का वातावरण शांत और ठंडा रखें
रात में भारी खाना न खाएँ
सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें या हल्का संगीत सुनें
Read Full Blog...
कई लोग बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं टाइप के होते हैं. इस तरह के लोगों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसे में कुछ टिप्स की मदद से आप जान सकते हैं किसकी पर्सनैलिटी कैसी है. किसी भी इंसान को पहचानना आसान नही होता कुछ लोग जैसे दिखते हैं असल में भी वैसे ही होते हैं और कुछ लोग जैसे दिखते हैं उनकी पर्सनैलिटी उसके विपरीत होती है. ऐसे में लोग कई बार धोखा खा जाते हैं. मगर अब परेशान होने की जरु...
Read More
कई लोग बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं टाइप के होते हैं. इस तरह के लोगों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसे में कुछ टिप्स की मदद से आप जान सकते हैं किसकी पर्सनैलिटी कैसी है.
किसी भी इंसान को पहचानना आसान नही होता कुछ लोग जैसे दिखते हैं असल में भी वैसे ही होते हैं और कुछ लोग जैसे दिखते हैं उनकी पर्सनैलिटी उसके विपरीत होती है. ऐसे में लोग कई बार धोखा खा जाते हैं. मगर अब परेशान होने की जरुरत नहीं है. साइकोलॉजी में कुछ टिप्स हैं जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं. वह इंसान काम करने में कैसा होगा आप इस बारे में भी इन टिप्स की मदद से जान सकते।
मानसिक परिश्रम
जो लोग कोई भी काम करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी चीज को करने से पहले सोचते हैं वह जीवन में ज्यादा सफल होते हैं. ऐसे लोग शारीरिक तौर पर ज्यादा काम करने वालों से जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं
सुबह जल्दी उठना
साइकोलॉजी का मानना है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वह ज्यादा एक्साइटेड होते हैं. उन्हें अपनी लाइफ में कुछ करना होता है और वह उसे करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं.
खराब हैंडराइटिंग
कई लोगों की हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लिखावट पढ़कर समझ नहीं आता है कि उन्होंने क्या लिखा है. साइकोलॉजी के मुताबिक जिस इंसान की राइटिंग बहुत खराब होती है वह बहुत इंटेलिजेंट होता है. उनकी सोचने की क्षमता भी ज्यादा तेज होती है.
ज्यादा बोलने वाले
कुछ लोगों को कम और काम से काम रखने तक बोलना पसंद होता है तो कुछ लोग लगातार घंटों तक बात कर सकते हैं. जो लोग घंटों तक बात कर सकते हैं वह कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए. साइकोलॉजी के अनुसार वह ज्यादा बोलने की वजह से अपना होश भी खोने लगते हैं. इसलिए हमेशा कम ही बोलना चाहिए
.
Read Full Blog...
स्टूडेंट के लिए Psychological Facts in Hindi About Study स्टडी से जुड़े कुछ ज़रूरी तथ्य इस प्रकार हैं: पढ़ाई के दौरान पिक्चर (फ़ोटो) के माध्यम से कोई व्यक्ति बेहतर अध्ययन कर सकता है। पढ़ाई शुरू करने से पहले, अपनी आंखें बंद कर लें और कवर किए जाने वाले चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स की कल्पना करें ताकि आप अपने दिमाग को ऊर्जा दे सकें। कई रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जो बच्चे अपने आहार में फल खाते हैं उनका आई...
Read More
स्टूडेंट के लिए Psychological Facts in Hindi About Study
स्टडी से जुड़े कुछ ज़रूरी तथ्य इस प्रकार हैं:
पढ़ाई के दौरान पिक्चर (फ़ोटो) के माध्यम से कोई व्यक्ति बेहतर अध्ययन कर सकता है।
पढ़ाई शुरू करने से पहले, अपनी आंखें बंद कर लें और कवर किए जाने वाले चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स की कल्पना करें ताकि आप अपने दिमाग को ऊर्जा दे सकें।
कई रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जो बच्चे अपने आहार में फल खाते हैं उनका आईक्यू दूसरों की तुलना में बेहतर होता है।
कोई भी व्यक्ति 30 मिनट से अधिक पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता है इसलिए नियमित अंतराल में छोटे-छोटे ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है। इससे आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं।
जब भी बड़े विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं तो उन विषयों को छोटे-छोटे खंडों में विभाजित करना बेहतर होता है।
माना जाता है कि पढ़ाई करते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठा जाए और अगर सुविधाजनक हो तो अपनी अध्ययन तालिका पूर्व दिशा में रखें।
अपने 60% नोट्स दिन के समय बनाने का प्रयास करें और उसी दिन उन्हीं नोट्स को दोहराने का प्रयास करें, इससे आपको आसानी से याद करने में मदद मिलती है।
सोने से पहले अपना 10 से 20 मिनट अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने में लगाएं, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है और आराम मिलता है।
ऐसा माना जाता है कि डार्क चॉकलेट आपको उच्च एकाग्रता में रहने में मदद करती है।
पढ़ाई के दौरान छात्र रात में कॉफी या गुनगुना पानी लें सकते हैं, जिससे नींद आने से बचने में मदद मिलती है।
अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग मामूली सवालों के जवाब में भी तुरंत व्यंग्य करते हैं, उनका दिमाग स्वस्थ रहता है।
स्टडी के अनुसार, जो लोग आपने उलटे हाथ से लिखते है वो अन्य लोगों की तुलना मे 3 वर्ष पहले मर जाते हैं।
95 प्रतिशत से अधिक लोग नया पेन खरीदने के बाद सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं।
नई चीजों को याद करने के लिए लगातार 30-40 मिनट तक पढ़ना चाहिए और फिर एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए।
रिपोर्ट और सर्वे के अनुसार ज्यादा किताबे पढ़ने वाला व्यक्ति दयालु हो जाता है।
एक जगह बैठकर पढ़ाई करने की तुलना मे जगह बदल कर पढ़ाई करना ज्यादा बेहतर माना जाता है।
कहा जाता है कि सोने से पहले 5 मिनट बुक्स रीड करने की आदत आपके जीवन को आसान बना देती है।
पढ़ाई के दौरान 70 प्रतिशत से अधिक स्टूडेंट्स को नींद आती है।
सस्टूडेंट्स किसी भी समय पढ़ाई कर सकते है पढ़ाई के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है।
ऐसा माना जाता है कि कोई भी नए विषय को याद करने के लिए उसे छोटे छोटे भागों मे बाटकर याद करने से वह विषय जल्दी याद हो जाता है।
एक शोध के अनुसार ये बताया गया है की दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले चीन में बच्चों को ज्यादा होमवर्क दिया जाता है
पढ़ते समय हर 20 से 30 मिनट बाद एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना चाहिए।
उम्मीद है कि आपको Psychological Facts in Hindi About Study का हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा।
Thank you ??
Read Full Blog...
स्वास्थ्य मनोविज्ञान स्वास्थ्य और कल्याण उद्योग में अध्ययन का एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है। यह इस बात का अध्ययन है कि लोग मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से दृष्टिकोण रखते हैं। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक ऐसी तकनीकों का उपयोग करते हैं जो लोगों को मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यदि आप स्वास्थ्य मनोविज्ञान को करियर के रूप में पढ़ने के इच्छु...
Read More
स्वास्थ्य मनोविज्ञान स्वास्थ्य और कल्याण उद्योग में अध्ययन का एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है। यह इस बात का अध्ययन है कि लोग मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से दृष्टिकोण रखते हैं। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक ऐसी तकनीकों का उपयोग करते हैं जो लोगों को मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
यदि आप स्वास्थ्य मनोविज्ञान को करियर के रूप में पढ़ने के इच्छुक हैं, तो आपको पहले इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप इस करियर पथ के लिए उपयुक्त हैं। यह तय करते समय कि यह आपके लिए सही करियर पथ है या नहीं, आपको कुछ बातों पर विचार करना चाहिए।
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक बनने के क्या लाभ हैं?
Q.1 स्वास्थ्य मनोविज्ञान एक अपेक्षाकृत नया करियर विकल्प और अध्ययन का क्षेत्र है
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान और स्वास्थ्य कैरियर के क्षेत्रों में एक अपेक्षाकृत नया पद है, इसलिए यह समझ में आता है कि इसे चुनना इतना आकर्षक विकल्प क्यों है। अध्ययन के नए नामित क्षेत्र में प्रवेश करना रोमांचक है क्योंकि इसमें नई खोज करने के कई अवसर होंगे।
यदि आप जिज्ञासु व्यक्ति हैं और नई चीजें सीखना पसंद करते हैं, तो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक बनना आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।
Q.2स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में नौकरियों की मांग अधिक है
स्वास्थ्य मनोविज्ञान एक नया और उभरता हुआ नौकरी का शीर्षक होने के कारण, इसकी मांग अधिक होने जा रही है। इस नौकरी के शीर्षक के नए होने के कारण, अध्ययन के इस क्षेत्र में बहुत से विशेषज्ञ नहीं होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि आप अभी इसके बारे में सीखना शुरू करते हैं, तो आप जल्दी ही एक विशेषज्ञ सलाहकार बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, 2020 और 2030 के बीच, स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में नौकरी की स्थिति में लगभग 8% की वृद्धि दर होने का अनुमान है ।
Q.3आपके पास स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में लोगों के जीवन में बदलाव लाने का अवसर है
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए मनोविज्ञान की शक्ति का उपयोग विज्ञान के रूप में करते हैं। वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में रुकावटों से जूझ रहे लोगों को शिक्षित करते हैं और उनकी सहायता करते हैं और ऐसा करके वास्तविक अंतर लाते हैं।
Q.4 आप एक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में एक अच्छा वेतन कमा सकते हैं
जो लोग स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में करियर का रास्ता अपनाते हैं, उनके पास अच्छा वेतन पाने की संभावना होती है। चूँकि स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक बनने के लिए बहुत व्यापक प्रशिक्षण और ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए अपनी सारी मेहनत, प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए अच्छी खासी रकम कमाना समझदारी होगी।
अमेरिका में एक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक $68,818 से $92,142 के बीच कमा सकता है , जिसका औसत वेतन लगभग $81,195 है।
Q.5 – एक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में आप विभिन्न संगठनों के साथ कई अलग-अलग सेटिंग्स में काम कर सकते हैं
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में आप कई अलग-अलग सेटिंग्स में काम कर सकते हैं। चाहे वह निजी प्रैक्टिस हो, अस्पताल हो या किसी अन्य प्रकार का मेडिकल क्लिनिक हो, स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक अक्सर ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जो दूसरों के उपचार और कल्याण को बढ़ावा देते हैं।
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक अक्सर किस प्रकार के कार्यक्रमों पर काम करते हैं, इसके प्रमुख उदाहरण हैं पुनर्वास और धूम्रपान छोड़ने में सहायता।
Q.6स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों को ढेर सारे आवश्यक शोध में भाग लेने और उन्हें संचालित करने में मदद करने का अवसर मिलता
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले शोध की भी हमेशा आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य देखभाल लागत को नियंत्रित करना स्वास्थ्य देखभाल नेताओं और रणनीति निर्माताओं के लिए आवश्यक है, जो कि शोध का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण तरीकों से योगदान दे सकते हैं।
वे स्वास्थ्य समस्याओं के कारणों और उनकी रोकथाम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या इस बात की जांच कर सकते हैं कि कुछ खास समूह के लोग जरूरत पड़ने पर देखभाल क्यों नहीं लेते।
वे रोगियों को प्रेरणा के साथ समझने और शांति पाने में मदद कर सकते हैं या उनके पूर्ण उपचार की संभावना बढ़ाने के लिए उपचार दिनचर्या का पालन करने में भी मदद कर सकते हैं।
Q.7एक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में, आपको दूसरों की वास्तव में मदद करने की संतुष्टि मिलती है
जीवन में लोगों की मदद करने की क्षमता होना वास्तव में आपके करियर से मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है। यह स्वास्थ्य मनोविज्ञान करियर क्षेत्र में विशेष रूप से सच है।
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक लोगों को खुद को ठीक करने और उनके लिए सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य-संबंधी विकल्प चुनने में मदद करते हैं। इसका उस व्यक्ति के जीने के तरीके पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और यह उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है।
यदि आप स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक बनना चुनते हैं, तो आपके पास लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे अवसर होंगे और ऐसा करने से आपको संतुष्टि भी मिलेगी।
Q.8आप एक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में अपने लिए स्वस्थ जीवन विकल्प चुनना जानेंगे
एक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में आप न केवल दूसरों को स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद कर पाएंगे, बल्कि आप खुद को भी अच्छे स्वास्थ्य विकल्प चुनने में मदद कर पाएंगे। यदि आप इसे एक कैरियर के रूप में चुनते हैं, तो आपको अपने लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य विकल्प चुनने में सक्षम होने के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा।
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ सुरक्षित और प्रभावी हों
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक चिकित्सा क्षेत्र में बीमारी और चोट की रोकथाम में भाग लेते हैं। वे रणनीतियाँ बनाते हैं और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों को तकनीक सिखाते हैं।
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति का एक और कर्तव्य अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाना है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रोगी को एक अच्छा अनुभव मिले और उसे सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सेवा मिले, जो जीवन रक्षक हो सकती है।
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक बनने के क्या नुकसान हैं?
विपक्ष नं. 1 - स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में लंबा समय लग सकता है
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आपको विश्वविद्यालय जाना होगा और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करनी होगी। मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में काफी समय लग सकता है। डॉक्टरेट की डिग्री सफलतापूर्वक प्राप्त करने में चार से छह साल तक का समय लग सकता है।
इसलिए, यदि आप स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक के रूप में अपना कैरियर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ाई पर काफी समय बिताने के लिए तैयार रहें।
विपक्ष संख्या 2 - स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों के लिए लाइसेंस हमेशा राज्यों के बीच हस्तांतरणीय नहीं होते हैं
एक बार जब आप एक राज्य में स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक बनने का लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, तो आप हमेशा यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह दूसरे राज्य में भी वैध रहेगा। इसलिए, जब तक आप राज्य से बाहर जाने की योजना नहीं बनाते हैं, तब तक यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नए राज्य में काम करने के लिए, आपको अपना लाइसेंस प्राप्त करने या उसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है।
राज्य के आधार पर, उस राज्य के कानून और वहां अभ्यास करने के नियमों के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त करना शीघ्र ही एक बड़ी समस्या न सकता है।
विपक्ष संख्या 3 - स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक बनने के लिए स्कूली शिक्षा सस्ती नहीं है
स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक बनने का एक और नुकसान यह है कि आपको कानूनी तौर पर मनोवैज्ञानिक बनने के लिए ज़रूरी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अध्ययन के इस क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम के लिए औसत ट्यूशन लगभग $132,200 है ।
इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक बनने के लिए वार्षिक शिक्षण शुल्क 22,000 से 33,000 डॉलर के बीच हो सकता है।
विपक्ष संख्या 4 – स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र की अपनी सीमाएँ हैं
स्वास्थ्य मनोविज्ञान अनुसंधान एक व्यापक क्षेत्र है, और इस पेशे के अंदर विभिन्न अध्ययनों के अलग-अलग फायदे और सीमाएं हैं।
स्वास्थ्य-संबंधी व्यवहार के तरीकों के बारे में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों की अनदेखी करने के लिए एचबीएम की निंदा की गई है।
साथ ही, यह विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी एक तरह का उपचार हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, और स्वास्थ्य मनोविज्ञान काफी सीमित हो सकता है और इसकी सीमाएँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति किसी भी स्वास्थ्य समस्या का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य मनोविज्ञान अनुकूल या प्रभावी नहीं लग सकता है।
Read Full Blog...
मनोविज्ञान मानव मन और उसके व्यवहार का विज्ञान और अध्ययन है। इसमें भावनाओं, चेतन और अचेतन घटनाओं और विचारों का अध्ययन शामिल है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। एक मनोवैज्ञानिक एक पेशेवर शोधकर्ता या व्यवसायी होता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं तक आसानी से पहुँचा जा सकता है और उन्हें जाना जा सकता है। यह मानवीय समस्याओं, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझने में मदद करता है। अध्ययन के इस क्षेत्...
Read More
मनोविज्ञान मानव मन और उसके व्यवहार का विज्ञान और अध्ययन है। इसमें भावनाओं, चेतन और अचेतन घटनाओं और विचारों का अध्ययन शामिल है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। एक मनोवैज्ञानिक एक पेशेवर शोधकर्ता या व्यवसायी होता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं तक आसानी से पहुँचा जा सकता है और उन्हें जाना जा सकता है। यह मानवीय समस्याओं, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझने में मदद करता है। अध्ययन के इस क्षेत्र में प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों को शामिल करते हुए बहुत अधिक गुंजाइश है। यह विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान की तुलना में बहुत व्यापक शब्द है। अध्ययन का यह क्षेत्र धारणा, भावना, ध्यान, व्यक्तित्व, प्रेरणा, अनुभूति, व्यक्तित्व, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और व्यवहार पर शोध करता है।
1.शब्द "मनोविज्ञान" किस भाषा से लिया गया है?
उत्तर. ग्रीक
व्याख्या: मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। साइकी का अर्थ है "जीवन" या "आत्मा"। लोगिया का अर्थ है "अध्ययन"। संक्षेप में, मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें व्यवहार, भावनाओं, चेतना और अचेतन मन का अध्ययन शामिल है।
2.मनोविज्ञान कितने प्रकार का होता है?
उत्तर . 4
व्याख्या : मनोविज्ञान के चार प्रकार हैं। ये इस प्रकार हैं: नैदानिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान हमें मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य और संबंधित परामर्श को समझने में मदद करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। व्यवहार मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कंडीशनिंग को जानना। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान मस्तिष्क, व्यवहार और उसके विकास का अध्ययन करने से संबंधित है।
3.मनोविज्ञान _____ और ______ का वैज्ञानिक अध्ययन है।
उत्तर: व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाएँ
व्याख्या : मनोविज्ञान अध्ययन का एक क्षेत्र है जो व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार को समझाता है। यह व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान और अध्ययन है। अध्ययन का यह क्षेत्र धारणा, भावना, ध्यान, व्यक्तित्व, प्रेरणा, अनुभूति, व्यक्तित्व, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और व्यवहार पर शोध करता है।
4.मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है?
उत्तर: सामाजिक विज्ञान
व्याख्या : मनोविज्ञान में, सामाजिक अनुभूति एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यह मानव मन और व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। मनोविज्ञान में सामाजिक व्यवहार, मानव विकास और भावनाओं का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान माना जाता है। यह एक विशिष्ट अध्ययन है जो अर्थशास्त्र, नृविज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान सहित अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग है।
5.प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक का नाम बताइए।
उत्तर: विल्हेम वुंड्ट
व्याख्या : विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंड्ट को प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रशंसित दार्शनिक, प्रोफेसर और जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1873 में पहली मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी लिखी थी। उन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की जहाँ उन्होंने प्रायोगिक मनोविज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने मानव मन और उसके कामकाज, धारणा और मानव की अन्य संज्ञानात्मक क्षमताओं को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का भी इस्तेमाल किया।
6.मस्तिष्क का कौन सा भाग अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करता है?
उत्तर: हिप्पोकैम्पस
व्याख्या: स्मृति मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पल क्षेत्र का एक प्राथमिक कार्य है। इसके लिए ग्रीक शब्द हिप्पोकैम्पस है, जहाँ हिप्पो का अर्थ है 'घोड़ा', और कैम्पोस का अर्थ है 'समुद्री घोड़ा' क्योंकि इसकी संरचना समुद्री घोड़े के समान है। दीर्घकालिक स्मृति का कार्य अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में जानकारी को समेकित करना है।
7.एक योग्य मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों वाले व्यक्तियों के इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को नियोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है -
उत्तर: मनोचिकित्सा ही इसका उत्तर है।
व्याख्या : मनोचिकित्सा को कभी-कभी बातचीत चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक उपचार के रूप में जाना जाता है। यह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का इलाज करने के लिए मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों या अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों के साथ बातचीत करने के लिए एक चिकित्सा शब्द है। मनोचिकित्सा मानसिक समस्याओं या व्यक्तित्व विकारों के इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक उपचारों का उपयोग करती है।
8.इनमें से कौन सा निदान योग्य निद्रा विकार नहीं है?
उत्तर: सोमनीलोक्वी
व्याख्या : सोमनीलोकी, जिसे अक्सर नींद में बात करना कहा जाता है, नींद में गड़बड़ी का एक प्रकार है। यह सोते समय जोर से बात करने को संदर्भित करता है। जो व्यक्ति सोता है वह इस बात से अनजान होता है कि वह सोते समय बात कर रहा है और वह इस बात से भी बेखबर होता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। यह काफी आम है और इसे आमतौर पर एक चिकित्सा स्थिति के रूप में नहीं देखा जाता
9.कौन प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है?
उत्तर. रीढ़ की हड्डी
व्याख्या : रीढ़ की हड्डी तंत्रिका कोशिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है। यह भावना और गति के लिए जिम्मेदार है। रीढ़ की हड्डी कई रिफ्लेक्स के लिए समन्वय केंद्र के रूप में भी काम करती है और इसमें रिफ्लेक्स आर्क होते हैं जो रिफ्लेक्स को अलग से नियंत्रित करते हैं।
10.कौन हमारे शरीर के अंगों की गति और स्थिति को समझ सकता है
उत्तर: प्रोप्रियोसेप्शन
व्याख्या : किनेस्थेसिया प्रोप्रियोसेप्शन का दूसरा नाम है। शरीर अपनी स्थिति, गति और घटकों का पता लगा सकता है। प्रोप्रियोसेप्शन को अपने पैरों को देखे बिना किक मारने या चलने की क्षमता या बंद आँखों से अपनी नाक को छूने में सक्षम होने से प्रदर्शित किया जा सकता है।
11.मस्तिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त करने का वह तरीका जो सामान्य मस्तिष्क गतिविधि को दर्शाता है, कहलाता है -
उत्तर: पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी
व्याख्या: PET या पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, मस्तिष्क को गतिशील अवस्था में दर्शाती है। PET चित्र सक्रिय मस्तिष्क क्षेत्रों को दर्शाते हैं। पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (PET) एक स्कैनिंग तकनीक है जो डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों को सर्जरी की आवश्यकता के बिना मस्तिष्क की जांच करने की अनुमति देती है।
12.रचनात्मकता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की?
उत्तर: गिलफोर्ड
व्याख्या: रचनात्मकता को नए विचारों को कल्पना करने और उन्हें जीवन में लाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड (जॉय पॉल गिलफोर्ड) संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। वह मानव बुद्धि की मनोवैज्ञानिक जांच पर अपने काम के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं।
Read Full Blog...
शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता अथवा आवश्यकता या महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैं-- 1. शिक्षा का बाल केन्द्रित होना आज की शिक्षा बाल केन्द्रित हो गई है। बालक की योग्यता, क्षमता, रूचि, अभिरूचि आदि के अनुसार पाठ्यक्रम, एवं प्रशिक्षण विधियों का निर्माण किया गया है। वर्तमान का छात्र शिक्षकों के कठोर नियंत्रण से मुक्त है। पाठ्यक्रम का निर्माण भी आज बाल केन्द्रित हो गया है 2....
Read More
शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता अथवा आवश्यकता या महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैं--
1. शिक्षा का बाल केन्द्रित होना
आज की शिक्षा बाल केन्द्रित हो गई है। बालक की योग्यता, क्षमता, रूचि, अभिरूचि आदि के अनुसार पाठ्यक्रम, एवं प्रशिक्षण विधियों का निर्माण किया गया है। वर्तमान का छात्र शिक्षकों के कठोर नियंत्रण से मुक्त है। पाठ्यक्रम का निर्माण भी आज बाल केन्द्रित हो गया है
2. बालक के सर्वोन्मुखी विकास मे योगदान देना
आज शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वोत्मुखी विकास करना है। शिक्षा-मनोविज्ञान इस विकास मे विशेष सहायक होता है। शिक्षा-मनोविज्ञान शिक्षक को उन सभी बातों का ज्ञान कराता है जिन-जिन अवस्थाओं और परिस्थितियों मे बालक का समुचित विकास हो सकता है।
3. उचित मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान प्रदान करने हेतु
अब यह सिद्ध हो चुका है कि परम्परागत परीक्षा प्रणालियों द्वारा बालक की क्षमताओं, व्यक्तित्व और शैक्षणिक उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन नही हो पाता। शिक्षा-मनोविज्ञान मूल्यांकन की आधुनिक, विश्वसनीय एवं प्रभावशाली विधियों की शिक्षक को पूर्ण जानकारी देता है जिसकी सहायता से वह बालकों के व्यक्तित्व और शैक्षणिक उपलब्धियों का सही-सही मूल्यांकन कर सकता है।
4. अनुशासन स्थापना में सहायक
शिक्षा-मनोविज्ञान, शिक्षक को अनुशासन स्थापित करने और रखने की अनेक नवीन विधियों और तकनीकों से अवगत कराता है।
5. अनुसंधान
नवीन अनुसंधान के द्वारा शिक्षक को नई-नई शिक्षण विधियों का परिचय प्राप्त होता है। इन विधियों के माध्यम से वह बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। इसमे शिक्षा-मनोविज्ञान की बहुत भूमिका होती है।
6. बालकों के लिये उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण
शिक्षा-मनोविज्ञान विभिन्न बातों का ज्ञान प्रदान करके शिक्षक को विभिन्न अवस्थाओं के छात्रों के लिये उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण करने मे सहायता देता है।
7. बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी
बालकों की रूचियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि मे अंतर होता है। शिक्षक को कक्षा मे ऐसे ही बालकों को शिक्षा देनी पड़ती है। अतः सफल शिक्षण के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी होना जरूरी है।
8. बालकों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण
शिक्षा-मनोविज्ञान विभिन्न बातों का ज्ञान प्रदान करके शिक्षक को विभिन्न अवस्थाओं के छात्रों के लिये उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण करने मे सहायता देता हैं।
9. सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान
शिक्षा-मनोविज्ञान शिक्षकों को अधिगम के नियमों से अवगत कराता है जिससे शिक्षक अधिक प्रखर हो जाता है तथा उसका ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ता हैं।
10. प्रेरणा
शिक्षा-मनोविज्ञान मे बालक के व्यवहार को समझने के लिए प्रेरणा एवं मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन का बहुत महत्व है, जिससे यह पता चलता है कि किसी प्रकार का व्यवहार बालक क्यों करता है, उनकी कौन-कौन सी आवश्यकताएं हैं।
11. व्यक्तिगत भिन्नता
छात्रों मे व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती है। सभी बालक सोचने-समझने की दृष्टि से सामान नही होते है। इनमें सोचने समझने की पृथका पाई जाती है। सभी की अपनी-अपनी योग्यताएँ एवं जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। मनोविज्ञान का आधार व्यक्ति है। शिक्षा-मनोविज्ञान के अनुसार बालकों की रूचि, क्षमताओं, स्तर, विकास, अभिरूचियों मे भिन्नता होती है।
12. कक्षा-शिक्षण की समस्याओं का समाधान
कक्षा-कक्ष की अनेक समस्यायें हैं-- अनुशासनहीनता, बाल-अपराध, समस्या बालक, बालकों का पिछड़ापन आदि। शिक्षा-मनोविज्ञान कक्षा-कक्ष की दैनिक समस्याओं का समाधान करने मे भी सहायता प्रदा नकरता है
13. बालकों की आवश्यकता का ज्ञान
छात्रों की विभिन्न आवश्यकतायें होती हैं जैसे-- प्रेम, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और किये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति। बालकों के समुचित विकास हेतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। शिक्षा-मनोविज्ञान शिक्षक को बालकों की इन आवश्यकताओं से अवगत कराता है।
Read Full Blog...
एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। कक्षा-शिक्षण और बालकों के दैनिक संपर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किये बिना वह अपने कार्य को कुशलता से संपन्न नही कर सकता है। अपने शिक्षण-कार्य को सफल बनाने तथा छात्रों के सीखने को लाभप्रद बनाने के लिये उसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिये। इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुये, एलिस क्रो ने यह वि...
Read More
एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। कक्षा-शिक्षण और बालकों के दैनिक संपर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किये बिना वह अपने कार्य को कुशलता से संपन्न नही कर सकता है। अपने शिक्षण-कार्य को सफल बनाने तथा छात्रों के सीखने को लाभप्रद बनाने के लिये उसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिये। इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुये, एलिस क्रो ने यह विचार व्यक्त किया कि," शिक्षकों को अपने शिक्षण मे उन मनौवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिये तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशील अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उनयोगिता अथवा आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हैं-
1. स्वयं को समझना
एक शिक्षक के लिए यह जानने जरूरी है कि उसमे अपने दायित्व के अनुकूल योग्यताएं है या नही। स्वभाव, बुद्धि, स्तर, जीवन दर्शन, स्वयं के निर्धारित मूल्य, शिक्षकों एवं अभिभावकों से संबंध, शिक्षक एवं छात्रों से संबंध, व्यवहार, चारित्रिक गुण, शिक्षक योग्यता की समाज में क्या प्रक्रिया हैं? शिक्षक का क्या दायित्व हैं? शिक्षक की क्या आवश्यकता हैं? आदि सभी बातों की जानकारी शिक्षक को शिक्षा-मनोविज्ञान की सहायता से मिल जाती हैं।
2. विद्यार्थी को जानना
एक शिक्षक को छात्र की समस्त शक्तियों एवं योग्यताओं की जानकारी होना जरूरी है। इसी के आधार पर वह अपने कार्य का संचालन करता है।
3. शिक्षण पद्धित
शिक्षा-मनोविज्ञान मे सीखने के लिए ऐसे अनेक सिद्धांत है जिनकी मदद से शिक्षक अपनी शिक्षण की विधियों का चयन कर सकते है एवं शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बना सकतें हैं।
4. विद्यार्थियों के मार्गदर्शन मे सहायक
उचित मार्गदर्शन के अभाव मे विद्यार्थी अपने पथ से भटक जाते हैं और उनके अध्ययन का उद्देश्य विफल हो जाता हैं। शिक्षा-मनोविज्ञान बालकों को समुचित दिशा प्रदान करता है जिससे वे अपनी क्षमताओं का समुचित ढंग से उपयोग करने में समर्थ हो जाते हैं।
5. शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक
शिक्षा-मनोविज्ञान शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने मे विशेष सहायक होता है। इस संबंध में स्किनर ने ठीक ही लिखा हैं," शिक्षा-मनोविज्ञान आजकल शिक्षक के जीवन को ज्ञान से समृद्ध कर उसकी शिक्षण विधि को उन्नत कर उसे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता हैं।"
6. शिक्षण विधियों के चयन मे सहायक
शिक्षा-मनोविज्ञान शिक्षकों को बालकों की आयु एवं स्तर तथा समय और परिस्थिति के अनुकूल शिक्षण विधि का चयन करने मे सहायता देता है क्योंकि प्रत्येक स्थिति और समय पर एक ही शिक्षण विधि को नही अपनाया जा सकता।
7. सीखने के लिए उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का आयोजन करना
शिक्षण कार्य के समय वातावरण एवं परिस्थितियों का भी शिक्षण की प्रक्रिया में एक विशेष महत्व होता है। शिक्षा-मनोविज्ञान के माध्यम से यह ज्ञात होता हैं, कि किस समय व्यक्तिगत शिक्षा तथा किस समय सामूहिक शिक्षण की आवश्यकता है, सहायक सामग्री का उचित प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। उपयुक्त परिस्थितियों शिक्षार्थी को सीखने के लिए अधिक प्रेरित करती हैं।
8. बाल-स्वभाव एवं व्यवहार का समुचित ज्ञान
शिक्षा-मनोविज्ञान शिक्षक को बालक के स्वभाव एवं व्यवहार से पूर्णतः अवगत कराता है। शिक्षक बालक की मूल प्रवृत्तियों और संवेग आदि की जानकारी भी प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान उसके शैक्षणिक और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में सहायक रहता हैं
9. मूल्यांकन
बालकों के मूल्यांकन के लिए बुद्धि, रूचि, व्यक्तित्व, ज्ञान आदि के शिक्षा मनोविज्ञान में अनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन कार्य में सबसे अधिक योगदान एक शिक्षक का होता है। इसलिए जरूरी है कि उसे शिक्षा-मनोविज्ञान की पूरी जानकारी हों।
10. मार्ग-निदर्शेन मे सहायता
शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को निर्देशन तथा परामर्श संबंधी सभी जरूरी तथ्यों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। अतः शिक्षा-मनोविज्ञान विद्यार्थियों के उचित मार्गदर्शन में अध्यापक की सहायता करता हैं।
11. बालक द्वारा विषय-वस्तु चयन मे सहायक
यह अध्यापक को ऐसी अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है जिससे वह बालक की मानसिक योग्यता, क्षमता, रूचि और रूझान के अनुसार विषय-वस्तु चयन करने एवं उन विषयों के शिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था करने में सहायक सिद्ध होता हैं।
12. सामाजिक भावना के विकास मे सहायक
शिक्षा-मनोविज्ञान अध्यापक को सामाजिक संबंधों के महत्व का ज्ञान कराता है। इसी ज्ञान के आधार पर अध्यापक सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करता है जो बालकों मे सामाजिक भावनाओं के विकास मे सहायक होता हैं।
13. शिक्षक के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाने में सहायक
शिक्षा-मनोविज्ञान शिक्षक/अध्यापक के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाता है जिसके फलस्वरूप वह शिक्षण-कार्य में आने वाली समस्याओं को सुलझाने एवं सही ढूँढने में सफल होता हैं।
14. शिक्षण पद्धितयों एवं तकनीकी से अवगत होना
यह शिक्षक (अध्यापक) को ऐसी पद्धतियों और तकनीकी से अवगत कराता है जिनके द्वारा वह अपने और दूसरे के व्यवहार का विश्लेषण कर बालक के व्यक्तित्व के समायोजन में सहायता देता हैं।
15. शिक्षण व्यवस्था को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना
शिक्षा-मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को विद्यालय प्रबन्ध, नियोजन और शिक्षण व्यवस्था करने हेतु मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता हैं।
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक को अपना शिक्षण प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा-मनोविज्ञान का अध्ययन करता अत्यंत ही आवश्यक हैं।
Read Full Blog...
सभी शिक्षा-मर्मज्ञों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक माना हैं। उनका कथन है कि यह विज्ञान अपनी विभिन्न खोजों हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तदुपरांत, यह उनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता बै तथा छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी करता हैं। जिस तरह वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण तथा परीक्षण करके उनके संबंध में अपने...
Read More
सभी शिक्षा-मर्मज्ञों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक माना हैं। उनका कथन है कि यह विज्ञान अपनी विभिन्न खोजों हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तदुपरांत, यह उनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता बै तथा छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी करता हैं। जिस तरह वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण तथा परीक्षण करके उनके संबंध में अपने निष्कर्ष निकालकर, किसी किसी सामान्य नियम का प्रतिपादन करता है, उसी तरह शिक्षक, कक्षा की किसी विशेष अथवा तात्कालिक समस्या का अध्ययन तथा विश्लेषण करके उसका समाधान करने का उपाय निर्धारित करता हैं। इस तरह, अपनी खोजों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने से शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञानों की श्रेणी में रखा गया हैं। हम अपने कथन के समर्थन में दो विद्वानों के विचारों को लेखबद्ध कर रहे हैं, यथा--
साॅरे तथा टेलफोर्ड," शिक्षा मनोविज्ञान, अपनी खोज के मुख्य उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता हैं।"
क्रो तथा क्रो के अनुसार," शिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान माना जा सकता हैं, क्योंकि यह मानव-व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक
विधि से निश्चित किये गये सिद्धांतों तथा तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करने का प्रयत्न करता हैं।"
शिक्षा मनोविज्ञान एक तरफ कार्य एवं कारण के संबंधों पर बल देता है, अतएव यह निष्कर्षों के प्रयोग को व्यावहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने हेतु प्रयत्न करने के कारण कला की श्रेणी में आता हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र (shiksha manovigyan ka kshera)
शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जो जीवन के वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होता है। यह एक आधुनिक मनोविज्ञान हैं। इसका क्षेत्र बहुत वृहद है। यही कारण है कि इसके क्षेत्र की सीमा तय करना आसान नही हैं। अनेक शिक्षा मनौवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए। जो इस प्रकार है--
क्रो एण्ड क्रो के अनुसार," शिक्षा मनोविज्ञान की विषय-सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से हैं।
स्किनर के शब्दों में," शिक्षा-मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित हैं, जो सीखने को प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक हैं।"
शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में हेरिस चेस्टर ने कहा हैं," शिक्षा-मनोविज्ञान का संबंध सीखने के मानवीय तत्व से है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रयोगसिद्ध मनोविज्ञानक सिद्धांतों का विनियोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता हैं। लेकिन यह ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें ऐसे प्रत्ययों की शिक्षा मे व्यवहार की परीक्षा तथा शिक्षकों की रूचि के निर्धारण के लिये प्रयोगात्मक कार्य किये जाते हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया और सीखने वाले को अधिकतम सुरक्षा और संतोष के साथ समाज में तादात्म्य स्थापित करने मे सहायता देने हेतु निर्देशित कार्यों का अध्ययन करना हैं।"
अमेरिकन वैज्ञानिक परिषद् ने मानव विकास, व्यक्तित्व तथा समायोजन, अधिगम, अध्ययन विधियों, मापन पद्धतियों आदि को शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया।
शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान सहायक होता है और यही सब समस्याएं व उनका समाधान शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र निर्धारित करती हैं।
उपरोक्त शिक्षा-मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत विचारों के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख रूप से निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता हैं--
1. मानव विकास
शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता हैं। जिसमें विकास की अवस्थाएं व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास सभी आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता हैं।
2. अधिगम प्रक्रिया
बालक के व्यवहार मे परिवर्तन करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य कार्य हैं। व्यवहार में यह बदलाव ही अधिगम कहलाता है। शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षण, अधिगम तथा अनुभवों के द्वारा सम्पन्न होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम की अवधारण, आधार, प्रकृति एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता हैं।
3. मापन एवं मूल्यांकन
शिक्षा-मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम बुद्धि, व्यक्तित्व आदि के मापन एवं मूल्यांकन से होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता हैं।
4. व्यक्तित्व
व्यक्तित्व (personality) आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वकथन भी किया जा सकता है। बालक का व्यक्तित्व उसकी मानसिक क्रियाओं तथा सामाजिक व्यवहार पर भी निर्भर करता है। शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले भौतिक तथा अभौतिक वातावरण व मानसिक योग्यता का अध्ययन करता है। इनके अलावा बालक की रूचियों, कल्पनाओं, संवेदनाओं और उसके सामाजिक व्यवहार को भी इसमें शामिल किया जाता है।
5. मानसिक स्वास्थ्य
मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा-मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता हैं। यदि छात्र मानसिक रूप से स्वस्थ नही होता है तो वह सीखने की स्थिति में नही होता है। फ्राॅयड के अनुसार," व्यक्ति के अचेतन मन की अधुरी इच्छाएं उसे मानसिक रूप से विचलित कर सकती हैं। मानसिक क्रियायें ही उसके व्यवहार को निरूपित करती है। समाज मे उचित समायोजन व तनाव, भग्नासा, संघर्ष तथा विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का संतुलित विकास होना बहुत ही जरूरी है। बालक का व्यवहार उसके अचेतन मन का ही परिणाम है। अतः शिक्षा-मनोविज्ञान व्यक्ति के अचेतन मन का भी अध्ययन करता है तथा इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक की कौन-कौन सी भावनाओं व इच्छाओं का दमन हुआ हैं।
6.बाल विकास
बाल विकास से अभिप्राय शिक्षण अधिगम द्वारा बालक के जैविक एवं मनोवैज्ञानिक विकास से हैं। बाल विकास का प्रमुख समय बाल्यावस्था के किशोरावस्था तक होता है। तथा इस समयावधि में बालक का संबंध शिक्षक, शिक्षण, शिक्षण संस्थाओं से अधिक रहता है। एक शिक्षक को यदि मनोविज्ञान की जानकारी होती है तो वह छात्र या छात्रों के इस विकासात्मक अवधि में अधिक सहायता प्रदान कर सकता है।
7. विशिष्ट बालक
विशिष्ट बालक वह होते है जो सामान्य नही होते जैसे-- प्रतिभाशाली, मंद-बुद्धि, शारीरिक दोष व मानसिक रूप से पिछ़डे बालकों को विशिष्ट की संज्ञा दी जाती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे बालकों का अलग से विवेचन करता है। इन बालकों मे सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ समानताएं एवं असमानताएं पाई जाती हैं। ऐसे बालक मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा शारीरिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। शिक्षा-मनोविज्ञान ऐसे बालकों के लिए उपयुक्त विधि का चुयन कर सावधानी से अध्ययन करता हैं।
8. पाठ्यक्रम निर्माण
शिक्षा-मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार से संबंधित सभी जानकारियाँ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जरूरी होती है। इन सब जानकारियों को एक क्रमबद्ध तरीके से जोड़कर शिक्षा-मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है
9. व्यक्तिगत भिन्नताएँ
व्यक्तिगत भिन्नताओं का छात्र अधिगम पर विशेष प्रभाव पड़ता है, सभी छात्रों की कुछ जन्मजात शक्तियाँ, पारिवारिक, सामाजिक आदि विशेषताएं होती है। शिक्षा-मनोविज्ञान का कार्य व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम कार्य को पूरा करना हैं। जैसे कुछ छात्र पढ़ाई में अच्छे होते हैं, किसी का प्रयोगात्मक ज्ञान अच्छा होता है, किसी का सैद्धांतिक ज्ञान अच्छा होता है, कोई चित्रकारी अच्छी करता है, कोई खेल मे अच्छा होता है, किसी की साहित्य मे रूचि होती हैं, किसी की कला में रूचि होती हैं, किसी को संगीत पसंद होता हैं इत्यादि। शिक्षक का कार्य व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना तथा उनके आधार पर शिक्षण-अधिगम कार्य करना होता हैं।
10. शारीरिक एवं मानसिक विकास
शारीरिक एवं मानसिक विकास शिक्षा-मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है। शिक्षा-मनोविज्ञान के अंतर्गत उचित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा छात्र के संपूर्ण विकास का प्रयास किया जाता है।
11. अनुसंधान
अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य बाल-व्यवहार एवं शिक्षण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का गहन अध्ययन कर उनका समाधान प्रस्तुत करना है ताकि इस क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किया जा सके। प्रामाणिक एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उचित विधियों के चुनाव में मदद करता हैं।
12. अध्ययन विधियाँ
इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न अध्ययन विधियों का विकास करना एवं उनको मान्यता प्रदान करना सम्मिलित है।
Read Full Blog...
वर्तमान मे शिक्षा को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने में मनोविज्ञान विशेष रूप से सहायक हो रहा है। इसी कारण इस बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षा का मुख्य आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। आज की शिक्षा पूरी तरह से बालकेन्द्रित है। इसका परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये है। यही कारण है कि शिक्षा का मूलाधार मनोविज्ञान हो गया है। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध हैं। मन...
Read More
वर्तमान मे शिक्षा को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने में मनोविज्ञान विशेष रूप से सहायक हो रहा है। इसी कारण इस बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षा का मुख्य आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। आज की शिक्षा पूरी तरह से बालकेन्द्रित है। इसका परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये है। यही कारण है कि शिक्षा का मूलाधार मनोविज्ञान हो गया है। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध हैं।
मनोविज्ञान मानव-व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव-व्यवहार मे परिवर्तन लाती है। इस प्रकार दोनों ही मानव जीवन से संबंधित है तथा दोनों का ही केन्द्र बिन्दु व्यक्ति है। वास्तव में मनोविज्ञान जहाँ मानव मन की गहराइयों मे पहुँचकर विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर मानव की अनुभूति और व्यवहार का तथ्यपूर्ण विश्लेषण करता हैं, वही शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव-व्यवहार में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन करती है और मानव-व्यवहार मे यह वांछित परिवर्तन मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर अधिक सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिये किये जाते हैं। इस तरह शिक्षा और मनोविज्ञान के परस्पर संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। आज की इस जटिल दुनिया मे बगैर मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा प्रदान करना संभव नही है। इस बात के संदर्भ में ड्रेवर का यह कथन सर्वथा उचित है कि," मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण तत्व है और बिना मनोविज्ञान की सहायता से हम शिक्षा की समस्याओं को हल नही कर सकते हैं। क्योंकि पाठ्य-सामग्री के चयन में, बालक की रूचियोंऔर क्षमताओं का ज्ञान कराने मे तथा बाल-व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान सहायक होता है। मनोविज्ञान सीखने के नियमो और सिद्धांतों का ज्ञान कराकर शिक्षा मे सीखने की प्रक्रिया को सजह बनाता है। बालकों के समुचित बौद्धिक एवं शारीरिक विकास मे भी मनोविज्ञान की अहम् भूमिका रहती है। अतः बिना मनोविज्ञान के सम्बद्ध हुये शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नही कर सकती। तभी तो स्किनर की यह मान्यता है कि 'शिक्षा का प्रमुख आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान है।'
शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंधों की विवेचना करते हुये ड्रेवर, स्किनर, डेविस, पेस्टालाजी, गेट्स व अन्य विद्वानों ने इस बात को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि शिक्षा और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध में डेविस का मत है कि," मनोविज्ञान के बालकों या विद्यार्थियों की विशेषताओं, क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में अपना योगदान दिया है।"
गेट्स व अन्य विद्वानों का कहना है कि," पाठ्य-विषयों का शिक्षण, शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निदान तथा निराकरण, शिक्षण उपलब्धियों का मापन, प्रौढ़ शिक्षा, शैक्षिक निर्देशन आदि इन सारी विशेष समस्याओं का निराकरण मनोविज्ञान के द्वारा होता हैं।"
मनोविज्ञान के शिक्षा संबंधी महत्व को स्वीकार करते हुये पेस्टालाजी ने लिखा हैं," शिक्षक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए और ज्ञान मनोविज्ञान के अध्ययन के अभाव में संभव नही हो सकता है।"
इसलिए शिक्षा और मनोविज्ञान का अटूट संबंध है और बिना मनोविज्ञान के शिक्षण-कार्य बहुत कठिन और अनुपयोगी हो सकता है।
निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति के अंदर 'व्यावहारिक परिवर्तन' लाये जाते हैं। मनोविज्ञान का संबंध इन्ही व्यावहारिक परिवर्तनों से हैं, जो व्यक्ति में शिक्षा के माध्यम से आते हैं। अतः हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दोनों का ही संबंध मानव-व्यवहार से हैं।
Read Full Blog...
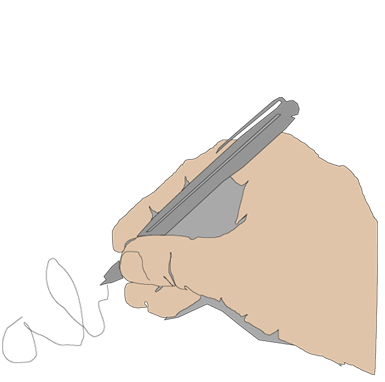 Digital Diary Submit Post
Digital Diary Submit Post