Blog by Motivation All Students | Digital Diary
" To Present local Business identity in front of global market"
" To Present local Business identity in front of global market"
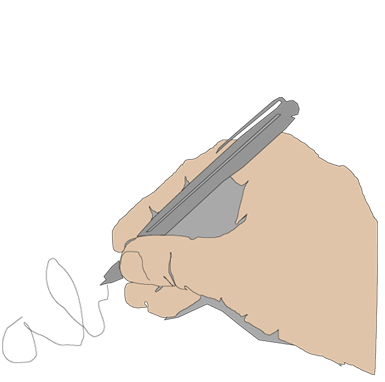 Digital Diary Submit Post
Digital Diary Submit Post
स्थान और महत्व: भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में भीमा नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह स्तंभ 1 जनवरी 1818 को हुए कोरेगांव की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की जीत की याद में बनाया गया था। इस लड़ाई में अधिकांश सैनिक महार जाति (दलित समुदाय) के थे, जिन्होंने पेशवा बाजीराव II की सेना को हराया था। यह स्तंभ दलित समुदाय के लिए सामाजिक गौरव और वीरता का प्रतीक बन गया है।
लड़ाई का कारण: पेशवा शासन (ब्राह्मणवादी व्यवस्था) के दौरान महार समुदाय को घोर जातिगत उत्पीड़न झेलना पड़ता था। पेशवा सैनिकों ने महारों को अछूत माना और उन पर अत्याचार किए।
ब्रिटिश सेना में महारों की भूमिका: ब्रिटिश सेना ने महार सैनिकों को अपनी रेजीमेंट में शामिल किया, क्योंकि उनकी वीरता और निष्ठा प्रसिद्ध थी।
लड़ाई का नतीजा: महार सैनिकों ने पेशवा की 28,000 सैनिकों वाली सेना के खिलाफ मात्र 500 सैनिकों के साथ जीत हासिल की।
स्थापना: 1821 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस स्तंभ का निर्माण कराया।
डिज़ाइन: स्तंभ की ऊँचाई लगभग 60 फीट है, जिस पर महार रेजीमेंट के 49 शहीद सैनिकों के नाम अंकित हैं।
शिलालेख: स्तंभ पर लिखा है – "इस स्थान पर ब्रिटिश सेना ने पेशवा की विशाल सेना को हराया, जो उनके साहस और अनुशासन का प्रमाण है।"
सामाजिक गौरव का प्रतीक:
महार सैनिकों की जीत को दलित समुदाय ने जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ विजय के रूप में देखा।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को इस स्थान का दौरा किया और इसे दलित अस्मिता का प्रतीक बताया।
वार्षिक समारोह (शौर्य दिवस):
हर साल 1 जनवरी को लाखों दलित यहाँ एकत्र होकर विजय स्तंभ को नमन करते हैं और सामाजिक न्याय की शपथ लेते हैं।
इस दिन को "दलित प्राइड डे" के रूप में मनाया जाता है।
बाइसेन्टेनियल सेलिब्रेशन: 1 जनवरी 2018 को कोरेगांव की लड़ाई के 200 साल पूरे होने पर एक बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ।
हिंसक झड़पें: कुछ समूहों ने जुलूस पर हमला कर दिया, जिससे हिंसा भड़क गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए।
कानूनी कार्रवाई: महाराष्ट्र पुलिस ने कथित तौर पर माओवादी संपर्कों के आरोप में कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिसे "भीमा कोरेगांव मामला" कहा गया।
दलित एकजुटता: यह स्तंभ दलितों को उनके इतिहास और वीरता की याद दिलाता है, जो उन्हें सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है।
सांस्कृतिक पुनर्जागरण: दलित साहित्य, कला, और संगीत में कोरेगांव की लड़ाई को सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है।
पर्यटन और शिक्षा: यह स्थल अब एक राष्ट्रीय स्मारक है, जहाँ देशभर से लोग इतिहास और सामाजिक न्याय के बारे में जानने आते हैं।
सुरक्षा चुनौतियाँ: 2018 की हिंसा के बाद से यहाँ भारी पुलिस बल तैनात रहता है, खासकर 1 जनवरी को।
भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ सिर्फ़ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि दलित अस्मिता, साहस, और संघर्ष का जीवंत प्रतीक है। यह समाज को याद दिलाता है कि "जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में इतिहास की भूमिका अमर है।" जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने कहा था: "शिक्षित बनो, संगठित रहो, और संघर्ष करो!"
Read Full Blog...भारत में दलित अधिकारों के लिए संघर्ष सदियों पुराना है, जो सामाजिक न्याय, समानता, और मानवीय गरिमा की लड़ाई का प्रतीक है। यह संघर्ष जातिवाद, छुआछूत, और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ एक सामूहिक आवाज़ बना। यहाँ इसके प्रमुख पड़ाव और नायकों की कहानी है:
ज्योतिबा फुले (1827-1890):
"सत्यशोधक समाज" (1873) की स्थापना करके दलितों और महिलाओं के शिक्षा के अधिकार की लड़ाई शुरू की।
"गुलामगिरी" (1873) किताब लिखकर जातिवाद की आलोचना की।
पेरियार ई.वी. रामासामी (1879-1973):
तमिलनाडु में "आत्मसम्मान आंदोलन" चलाया, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ था।
महाड़ सत्याग्रह (1927):
महाराष्ट्र के महाड़ में चवदार तालाब से दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाया।
मनुस्मृति दहन (25 दिसंबर 1927) के ज़रिए जातिवादी ग्रंथों का विरोध किया।
पूना पैक्ट (1932):
गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता, जिसमें दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई।
संविधान निर्माण (1947-1950):
अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 (छुआछूत उन्मूलन), अनुच्छेद 15-16 (समानता) जैसे प्रावधान जोड़े।
दलित पैंथर्स (1972):
महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल और राजा ढाले ने दलित पैंथर्स की स्थापना की, जो साहित्य और आंदोलनों के माध्यम से जागरूकता फैलाई।
मंडल आयोग (1990):
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने की सिफारिशों के लिए हुए आंदोलनों ने दलित-बहुजन एकता को मजबूत किया।
भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ (2018):
महाराष्ट्र में दलित समुदाय ने ब्रिटिश सेना में लड़े महार योद्धाओं की याद में जुटकर सामाजिक गौरव का प्रदर्शन किया।
छुआछूत विरोधी कानून (1955):
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम (अब SC/ST एक्ट) लागू हुआ, जो दलितों के खिलाफ भेदभाव को दंडित करता है।
रोहित वेमुला की आत्महत्या (2016):
हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की मौत ने शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर बहस छेड़ी।
उना आंदोलन (2016):
गुजरात में दलित युवाओं की पिटाई के विरोध में हुए प्रदर्शनों ने देशभर में सामाजिक न्याय की मांग को तेज़ किया।
साहित्यिक विद्रोह:
ओमप्रकाश वाल्मीकि ("जूठन"), बामा फ़ातिमा ("करुक्कु"), और मराठी लेखक बाबुराव बागुल ने दलित जीवन की पीड़ा को शब्द दिए।
जनजागरण के प्रतीक:
भीम जयंती (14 अप्रैल) और महाराष्ट्र का "विजय दशमी" (मनुस्मृति दहन दिवस) दलित गर्व के प्रतीक बने।
जातिगत हिंसा:
खैरलांजी (2006), उत्तर प्रदेश का हाथरस मामला (2020) जैसी घटनाएँ दलित सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं।
शिक्षा और रोज़गार:
आरक्षण नीतियों के बावजूद दलितों तक उच्च शिक्षा और नौकरियों में समान पहुँच अभी भी एक लक्ष्य है।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व:
दलित नेता मायावती, चंद्रशेखर आजाद "रावण", और जिग्नेश मेवाणी आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।
दलित अधिकारों का संघर्ष न सिर्फ़ कानूनी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की मांग करता है। डॉ. अंबेडकर के शब्दों में: "राजनीतिक सत्ता समाज की बुराइयों का इलाज नहीं है। समाज को नैतिक बनाना होगा।" यह संघर्ष आज भी जारी है, क्योंकि "समानता का अधिकार अभी अधूरा है।"
Read Full Blog...पृष्ठभूमि: मनुस्मृति (या मानव धर्मशास्त्र) एक प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ है, जिसे लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया माना जाता है। यह ग्रंथ सामाजिक व्यवस्था, जाति-व्यवस्था, और स्त्री-पुरुष के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसमें दलितों और महिलाओं के प्रति अपमानजनक और असमान नियमों का उल्लेख है, जिसके कारण यह सदियों से सामाजिक भेदभाव का प्रतीक बना रहा।
तिथि और स्थान: 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ शहर में।
नेतृत्व: डॉ. भीमराव अंबेडकर और उनके सहयोगियों ने इसका आयोजन किया।
संदर्भ: यह घटना महाड़ सत्याग्रह का हिस्सा थी, जिसमें दलितों को सार्वजनिक तालाब (चवदार तालाब) से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया गया।
जातिगत असमानता का विरोध:
मनुस्मृति में दलितों को "अछूत" और शूद्रों को निम्न स्थान देने वाले नियमों का सार्वजनिक रूप से विरोध करना।
अंबेडकर का कहना था: "मनुस्मृति भारतीय समाज की बेड़ियाँ हैं, जिन्हें तोड़ना ज़रूरी है।"
सामाजिक चेतना जगाना:
दलित समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाना।
प्रतीकात्मक क्रांति:
ग्रंथ को जलाना एक प्रतीकात्मक कार्य था, जो यह संदेश देता था कि समाज को जातिवाद और असमानता पर आधारित ग्रंथों को नकारना चाहिए।
सभा का आयोजन: महाड़ में हज़ारों दलितों और सुधारवादियों की एक सभा हुई।
मनुस्मृति की प्रतियाँ जलाई गईं: अंबेडकर ने कहा, "यह ग्रंथ हमें गुलाम बनाता है, इसे आग के हवाले करो!"
ऐतिहासिक भाषण: अंबेडकर ने कहा, "मनुस्मृति ने हमें सदियों से दबाया है। आज हम इसकी आग में अपनी आज़ादी की लौ जलाएँगे!"
रूढ़िवादियों का विरोध:
कट्टरपंथी समूहों ने इस घटना की निंदा की और अंबेडकर को हिंदू धर्म का "दुश्मन" बताया।
दलित चेतना का उभार:
यह घटना दलितों के लिए गर्व और आत्मसम्मान का प्रतीक बनी।
इसके बाद देशभर में जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन तेज़ हुए।
संविधान निर्माण की नींव:
अंबेडकर के इस संघर्ष ने भारतीय संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने की राह बनाई।
प्रथम सार्वजनिक विद्रोह: यह पहली बार था जब किसी धार्मिक ग्रंथ को सामाजिक अन्याय के प्रतीक के रूप में जलाया गया।
बौद्धिक क्रांति का प्रतीक: अंबेडकर ने दिखाया कि शिक्षा और तर्क के बल पर पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी जा सकती है।
आधुनिक भारत की प्रेरणा: यह घटना आज भी सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले समूहों के लिए प्रेरणास्रोत है।
उन्होंने कहा था: "मनुस्मृति को जलाना कोई धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि मानवता के नाम पर एक नैतिक कर्तव्य है।"
उनका लक्ष्य था: "ऐसा समाज बनाना, जहाँ हर व्यक्ति को उसकी मेहनत और योग्यता के आधार पर सम्मान मिले।"
निष्कर्ष: मनुस्मृति दहन सिर्फ़ एक ग्रंथ को जलाने की घटना नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का ऐलान था। यह आज भी उन लोगों के लिए मशाल की तरह है, जो जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लड़ते हैं।
Read Full Blog...जन्म और प्रारंभिक जीवन: डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू (तब मध्य भारत, अब डॉ. अंबेडकर नगर) में एक गरीब दलित (महार जाति) परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे, और माता भीमाबाई एक गृहिणी थीं। जातिगत भेदभाव के कारण बचपन से ही उन्हें सामाजिक अपमान और अलगाव झेलना पड़ा।
प्रारंभिक शिक्षा:
स्कूल में उन्हें "अछूत" मानकर अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए छूत के डर से कोई मदद नहीं करता था।
1907 में मैट्रिक पास करने वाले पहले दलित छात्र बने।
उच्च शिक्षा:
1913 में बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, और अंग्रेजी सहित 9 भाषाओं के ज्ञाता थे।
दलित अधिकारों के लिए संघर्ष:
1927 में महाड़ सत्याग्रह चलाया, जहाँ दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया।
1930 में नाशिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया।
मनुस्मृति दहन:
1927 में ही उन्होंने मनुस्मृति (जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है) का सार्वजनिक रूप से दहन किया।
पूना पैक्ट (1932):
गांधी जी के साथ हुए इस समझौते में दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के बजाय आरक्षण की व्यवस्था की गई।
संविधान निर्माता:
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया।
संविधान में समानता, स्वतंत्रता, और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल कर दलितों, महिलाओं, और श्रमिकों के अधिकार सुनिश्चित किए।
14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया।
उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता और तर्क पर आधारित है, जो जातिवाद को खत्म कर सकता है।
"जाति का विनाश" (Annihilation of Caste)
"भारत का राष्ट्रीय विभाजन" (Pakistan or Partition of India)
"बुद्ध और उनका धम्म"
6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया।
उन्हें भारत रत्न (1990, मरणोपरांत), "बाबासाहेब" और "संविधान निर्माता" के सम्मान से जाना जाता है।
14 अप्रैल को उनके जन्मदिन को "भीम जयंती" के रूप में मनाया जाता है, जो भारत में एक सार्वजनिक अवकाश है।
"शिक्षित बनो, संगठित रहो, और संघर्ष करो।"
"मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता, और भाईचारा सिखाए।"
"राजनीतिक सत्ता समाज की बुराइयों का इलाज नहीं है। सामाजिक बुराइयों को खत्म करना ज़रूरी है।"
डॉ. अंबेडकर की विरासत आज भी भारत में सामाजिक न्याय, शिक्षा, और दलित उत्थान के प्रतीक के रूप में जीवित है। उनके समर्थक उन्हें "आधुनिक भारत का मसीहा" मानते हैं।
Read Full Blog...